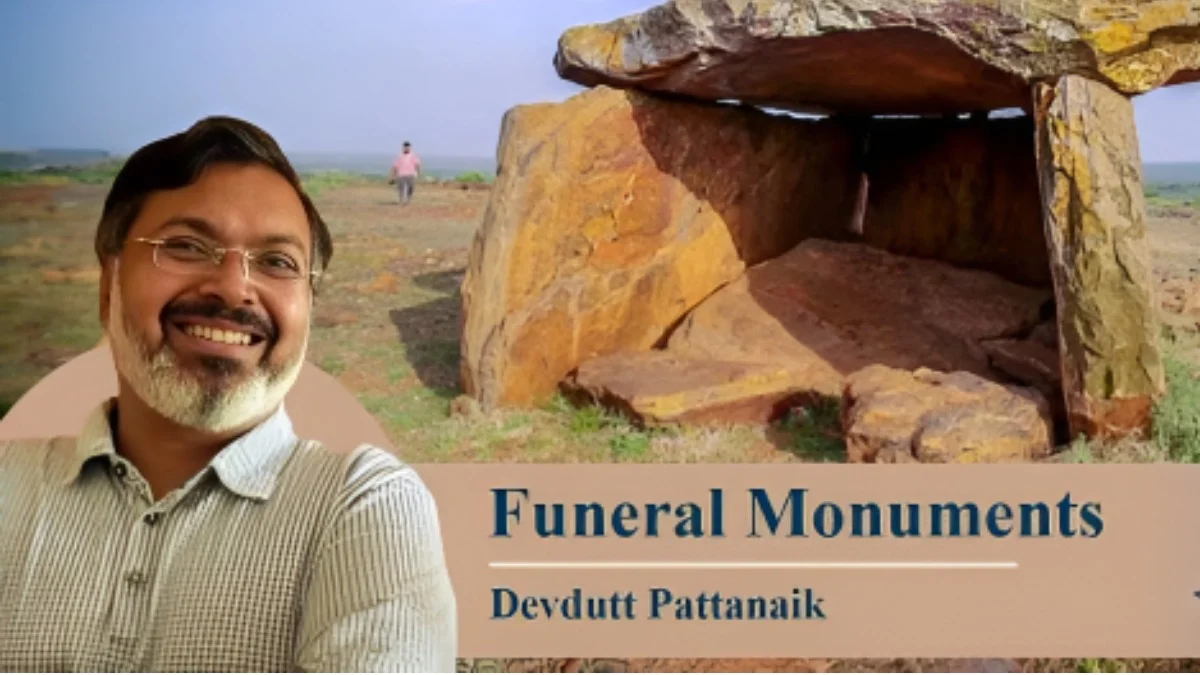Devdutt Pattanaik on Arts and Culture: (द इंडियन एक्सप्रेस ने UPSC उम्मीदवारों के लिए इतिहास, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कला, संस्कृति और विरासत, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी आदि जैसे मुद्दों और कॉन्सेप्ट्स पर अनुभवी लेखकों और स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए लेखों की एक नई सीरीज शुरू की है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ें और विचार करें और बहुप्रतीक्षित UPSC CSE को पास करने के अपने चांस को बढ़ाएं। इस लेख में, पौराणिक कथाओं और संस्कृति में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपने लेख में भारत में अलग-अलग धर्मों में होने वाली अंतिम संस्कार की प्रथाओं पर चर्चा की है।)
किसी भी समाज में अलग-अलग संस्कृतियां परलोक की अलग-अलग कल्पना करती हैं और इसलिए अंतिम संस्कार की प्रथाएं भी अलग-अलग होती हैं। आमतौर पर एक जीवन में विश्वास करने वाले लोग शवों को कब्रों में रखते हैं और दफ़न स्थलों पर क़ब्र के पत्थर लगाते हैं। इसी तरह पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग शरीर को प्रकृति में विलीन कर देते हैं। वे इसे विलीन करने के लिए आग, जल या जंगली जानवरों की प्रक्रिया को अपनाते हैं।
क्या है ब्राह्मी लिपि का इतिहास, कैसे हुई इसकी शुरुआत? देवदत्त पटनायक से इसके बारे में जाने सबकुछ
असम में 13वीं शताब्दी में दक्षिण-पूर्व एशिया के रास्ते चीन से आए अहोम राजा, मृतकों को मोइदम नामक टीलों में दफनाते थे। कभी-कभी राजाओं के साथ उनके सेवकों या अन्य लोगों को भी दफनाया जाता था। जब वे हिंदू बन गए और दाह संस्कार की प्रथा अपनाने लगे, तो यह प्रथा बदल गई। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, पुनर्जन्म के लिए अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस प्रकार अंतिम संस्कार की प्रथाओं में बदलाव संस्कृति में बदलाव को दर्शाता है।
प्रागैतिहासिक काल में बर्तन दफ़नाने का अभिन्न अंग थे। प्राथमिक तौर पर दफ़नाने में प्राचीन लोग मृतकों को बर्तनों में दफ़नाते थे। द्वितीयक दफ़नाने में बर्तनों में दाह संस्कार के बाद एकत्रित अस्थियाँ रखी जाती थीं। तमिल संगम काव्य में एक विधवा द्वारा कुम्हार से अपने मृत पति के लिए एक बड़ा बर्तन बनाने का उल्लेख भी मिलता है। दफ़नाने वाले प्रागैतिहासिक स्थलों में ‘सिस्ट’ भी पाए जाते हैं, जो पत्थरों से बने गड्ढे होते हैं, जो आमतौर पर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं।
बरगद से लेकर ब्रेडफूट तक, अलग-अलग राज्यों के स्पेशल पेड़ों का भी है संस्कृतिक महत्व
हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार तो होता था लेकिन कई समुदाय मृतकों को दफनाते थे। हड़प्पा में ऐसे कब्रिस्तान मिले हैं, जहां लोगों के पास बहुत कम दफ़नाने का सामान जैसे मनके और कुछ बर्तन था। इसके अलावा धोलावीरा में ऐसे टीले हैं, जहां कोई शव नहीं हैं शायद ये उन लोगों की याद में बनाए गए थे जो दूर देशों की यात्रा करते समय मारे गए थे।
दक्कन क्षेत्र के महापाषाण लौह युग (1000 ईसा पूर्व) के समाधि स्थलों से संबंधित हैं। महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता है, ये उस समय जब वैदिक संस्कृति गंगा-यमुना नदी घाटी में फल-फूल रही थी। समाधि स्थलों पर दो ऊर्ध्वाधर पत्थरों से एक मंदिर बनाया जाता था, जिसके ऊपर एक शीर्षशिला क्षैतिज रूप से रखी जाती थी, जिसे डोलमेन कहा जाता है। इस संरचना के नीचे मृतकों की स्मृति में अस्थियाँ और खाद्य पदार्थ रखे जाते थे।
वेदों में दाह संस्कार और दफ़नाने, दोनों ही प्रथाओं का उल्लेख है। रामायण और महाभारत , दोनों में दाह संस्कार का उल्लेख मिलता है। दशरथ का दाह संस्कार किया गया। रावण का दाह संस्कार किया गया। कौरवों का दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों में मृतक, अर्थात् पितृ को भोजन कराना शामिल था।
भारत ने कैसे पूर्व-पश्चिम को जोड़ने में निभाई अहम भूमिका, देवदत्त पटनायक ने शेयर की कहानियां
अंतिम संस्कार आमतौर पर उच्च जातियों के समुदायों में होते हैं, जो लकड़ी का प्रबंध कर सकते हैं। कई निम्न जातियों के समुदाय आज भी पूर्व-वैदिक दफ़नाने की प्रथाओं का पालन करते हैं। दफ़नाने का कार्य अक्सर परिवार के स्वामित्व वाले खेतों में किया जाता है ताकि स्वामित्व और स्वामित्व का संकेत मिल सके।
भारत के कई हिस्सों में लोगों को बैठी हुई अवस्था में ही दफनाया जाता था, खासकर अगर वे किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित होते थे। ऐसा माना जाता था कि किसी धार्मिक समुदाय से जुड़े लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता। कई हिंदू मठों में, संत को बैठी हुई अवस्था में ही दफनाया जाता था और उसके ऊपर एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए गमले में तुलसी लगाई जाती थी।
जैन भिक्षुओं की कब्र पर अक्सर एक पेड़ लगाया जाता था या उसके ऊपर एक स्तूप बनाया जाता था। दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों पर स्तूप बनाने की प्रथा बौद्धों द्वारा भी अपनाई जाती थी। वास्तव में वैदिक लोग बौद्धों को अस्थि पूजक मानकर उनकी निंदा करते थे। शरीर या अस्थियों को दफ़नाने वाले बौद्ध स्थलों को स्तूप कहा जाता था, जबकि हिंदू और जैन स्थलों को समाधि कहा जाता था।
सुल्तान, बादशाह और शहंशाह: ये उपाधियां भारत के मुस्लिम शासकों के बारे में क्या कहती हैं?
समाधि स्थल बनाए जाते थे जहाँ दफ़नाने या दाह संस्कार स्थल को एक मंदिर द्वारा चिह्नित किया जाता था और उस पर शिवलिंग की एक प्रतिमा स्थापित की जाती थी। कुछ चोल राजाओं द्वारा इसका प्रचलन था। राजस्थान, गुजरात और भारत के कई हिस्सों में वीर शिलाओं का उपयोग उस स्थान को चिह्नित करने के लिए किया जाता था, जहां कोई योद्धा गांव को हमलावरों या जंगली जानवरों से बचाते हुए शहीद हुआ था। सती शिलाओं का उपयोग उन स्थानों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था, जहां स्त्रियां अपने पतियों की चिता पर आत्मदाह करती थीं। कर्नाटक में निशिधि शिलाओं का उपयोग उन स्थानों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था जहां जैन मुनियों ने मृत्युपर्यन्त उपवास किया था।
मकबरे बनाने की शुरुआत दसवीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लामी संस्कृति के आगमन के साथ हुई लेकिन मकबरे बनाना कोई अरबी प्रथा नहीं है बल्कि, यह मध्य एशिया से आई है। अरब लोग मृतकों को दफ़नाते थे, और प्राचीन पारसी लोग अपने मृतकों को प्राकृतिक वातावरण और गिद्ध जैसे जंगली पक्षियों के सामने छोड़ देते थे। मध्य एशियाई जनजातियों, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्हें भी मकबरे बनाने का शौक था और उन्होंने भारत में स्मारकीय मकबरों का निर्माण शुरू किया। इसलिए, दसवीं शताब्दी के बाद, हमें भारत में खिलजी, तुगलक, लोदी और सूरी के मकबरे मिलते हैं और उसके बाद प्रसिद्ध मुगल स्मारक ताजमहल भी है।
Art and Culture with Devdutt Pattanaik: संस्कृति को समझने के लिए मिट्टी के बर्तन क्यों हैं जरूरी?
इस मुस्लिम प्रथा का पालन करते हुए, कई राजपूतों ने शाही दाह-संस्कार स्थल पर गुंबद और मंडप बनवाना शुरू कर दिया। इन्हें क्षत्रियां कहा जाता था। कुछ क्षत्रियां महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती हैं। यह प्रथा 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। आज भी जिन स्थानों पर राजनीतिक नेताओं का दाह-संस्कार किया जाता है, वहां ‘समाधियां’ बनाई जाती हैं। यह वैदिक मान्यता के विरुद्ध था कि पुनर्जन्म की सुविधा के लिए मृतक का कोई निशान नहीं रखा जाना चाहिए।
पूर्वोत्तर भारत में मोनपा जैसे आदिवासी समुदाय हैं, जहां शवों को 108 टुकड़ों में काटकर नदियों में फेंक दिया जाता है ताकि मछलियाँ उन्हें खा जाएं। इस प्रकार, भारत भर में अंतिम संस्कार स्मारकों का अध्ययन देश की विविध धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
IAS और IPS के इतने पद पड़े हैं खाली, जानें राज्यसभा में मोदी सरकार के दिए हुए आंकड़ों की जानकारी
(देवदत्त पटनायक एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाकार हैं जो कला, संस्कृति और विरासत पर लिखते हैं।)
हमारे UPSC न्यूज़लेटर की सदस्यता लें और पिछले हफ्ते के समाचार संकेतों से अपडेट रहें।
हमारे टेलीग्राम चैनल – इंडियनएक्सप्रेस यूपीएससी हब से जुड़कर यूपीएससी के लेटेस्ट लेखों से अपडेट रहें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करें।